

अर्जुन उवाच |
सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् |
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन || 1||
अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कहा; संन्यासस्य-कर्मों का त्याग; महाबाहो-बलिष्ठ-भुजाओं वाला; तत्त्वम्-सत्य को; इच्छामि चाहता हूँ; वेदितुम्–जानना; त्यागस्य-कर्मफल के भोग की इच्छा का त्याग; च-भी; हृषीकेश–इन्द्रियों के स्वामी, श्रीकृष्ण; पृथक्-भिन्न रूप से; केशि-निषूदन-केशी असुर का संहार करने वाले, श्रीकृष्ण।
BG 18.1: अर्जुन ने कहा-हे महाबाहु। मैं संन्यास और त्याग के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशिनिषूदन, हे हृषीकेश! मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ।
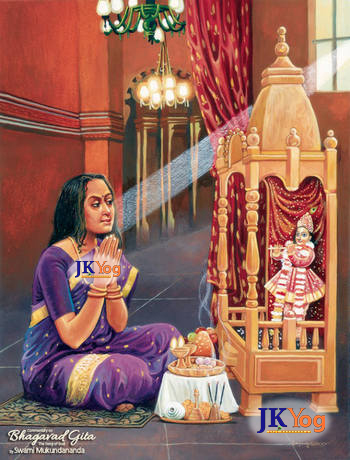
Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!
अर्जुन, श्रीकृष्ण को 'केशिनिषूदन' कहकर संबोधित करता है जिसका अर्थ केशी नामक असुर का संहार करने वाला है। भगवान श्रीकृष्ण ने केशी नामक असुर का वध किया था जिसने एक पागल घोड़े का रूप धारण करके ब्रिजभूमि में आतंक मचा रखा था। संशय भी एक बे-लगाम घोड़े के समान है जो मन-मस्तिष्क में निरंतर दौड़ लगाता रहता है तथा भक्ति की फुलवारी को नष्ट कर देता है। अर्जुन इंगित करता है कि "जैसे आपने केशी नामक राक्षस का वध किया था उसी प्रकार मेरे मन-मस्तिष्क में उठने वाले संशय का भी दमन कीजिए।" अर्जुन का प्रश्न अत्यंत मार्मिक है। वह संन्यास की प्रकृति के बारे में जानना चाहता है जिसका अर्थ 'कर्मों का त्याग' करना है। वह त्याग की प्रकृति जिसका अर्थ 'कर्म-फलों को भोगने की इच्छाओं का त्याग करने से है' के संबंध में भी जानना चाहता है। आगे वह 'पृथक्' शब्द का प्रयोग करता है जिसका अर्थ भिन्नता है। अतः वह इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर को भी जानना चाहता है।
अर्जुन श्रीकृष्ण को "हृषीकेश" कह कर संबोधित कर रहा है जिसका अर्थ "इन्द्रियों का स्वामी" है। अर्जुन का लक्ष्य महाविजय करना है, जिसे मन और इन्द्रियों को वश में करके ही संपूर्ण किया जा सकता है। यह वही विजय अभियान है जिससे पूर्ण शांति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पुरुषोतम भगवान श्रीकृष्ण स्वयं इसके प्रमाण हैं।
इस संबंध में पिछले अध्यायों में भी वर्णन किया जा चुका है। श्लोक 5.13 तथा 9.28 में श्रीकृष्ण संन्यास के संबंध में और श्लोक 4.20 तथा 12.11 में त्याग के बारे में वर्णन कर चुके थे।लेकिन यहाँ पर वे इसे अन्य दृष्टिकोण से निरूपित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ एक उद्यान के विभिन्न हिस्से हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न करते हैं जबकि पूरा उद्यान सम्मिलित रूप से एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भगवद्गीता भी कुछ इसी प्रकार से है। प्रत्येक अध्याय को एक योग रूप में निर्दिष्ट किया गया है तथा अठारहवें अध्याय को पूरी भगवद्गीता का सार कहा जा सकता है। इस अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण संक्षिप्त रूप में मूलभूत सिद्धांतों तथा सत्य का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें पिछले 17 अध्यायों में भी प्रस्तुत किया गया था। अब वे सबका सकल निष्कर्ष स्थापित करते हैं। संन्यास तथा विरक्ति के विषयों पर चर्चा करने के उपरांत भगवान श्रीकृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं और यह बतलाते हैं कि किस प्रकार से ये जीवात्माओं के कार्यों को प्रभावित करते हैं। वे पुनः कहते हैं कि केवल सत्त्वगुण को पोषित करना ही उपयुक्त है। तत्पश्चात् वे यह निष्कर्ष देते हैं कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति ही हमारा परम कर्त्तव्य है और इसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है।